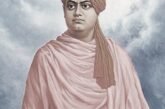हाल ही में देश में स्कूलों के संदर्भ में जारी किए गए आंकड़े हैरानी पैदा करने वाले हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार देशभर में लगभग 7,993 स्कूलों में एक भी छात्र का नामांकन नहीं हुआ है, जबकि इन स्कूलों में 20,817 शिक्षक अब भी कार्यरत हैं। कितनी बड़ी बात है कि लगभग 8 हजार स्कूलों में बीस हजार से भी ज्यादा शिक्षक कार्यरत हैं और वहां एक भी छात्र का नामांकन नहीं है।

दरअसल, जो आंकड़े सामने आए हैं, वे वर्ष 2024–25 के शैक्षणिक सत्र से संबंधित है। आंकड़े बताते हैं कि सबसे अधिक शून्य नामांकन वाले स्कूल पश्चिम बंगाल में पाए गए हैं, जहाँ 3,812 स्कूलों में एक भी छात्र दर्ज नहीं है, जबकि इनमें 17,965 शिक्षक तैनात हैं। इसके बाद तेलंगाना में 2,245 और मध्य प्रदेश में 463 ऐसे स्कूल दर्ज किए गए हैं। वहीं अच्छी बात यह है कि हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, असम, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा और दिल्ली जैसे राज्यों में ऐसे कोई स्कूल नहीं पाए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष यानी 2023–24 में लगभग 12,954 स्कूलों में नामांकन शून्य था, जो अब घटकर 8,000 के आसपास रह गया है। मंत्रालय ने राज्यों को सलाह दी है कि ऐसे स्कूलों को पास के विद्यालयों में मिलाया जाए या उनके संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि शिक्षकों और अधोसंरचना का बेहतर प्रबंधन हो सके। कहना ग़लत नहीं होगा कि यह स्थिति देश में शिक्षा संसाधनों के असमान वितरण और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति घटती रुचि को भी दर्शाती है।
 दरअसल,देश में शिक्षा संसाधनों के असमान वितरण और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति रुचि के अभाव के पीछे कई गहरे और आपस में जुड़े हुए कारण हैं। मसलन, जहां शिक्षा संसाधनों के असमान वितरण की बात है तो आज शहरों में बहुत से अच्छे स्कूल स्थित हैं, उनमें बच्चों के लिए आधुनिक सुविधाएं व अच्छा स्टाफ उपलब्ध है। वहीं दूसरी ओर गांवों के स्कूलों में संसाधन बहुत ही सीमित हैं। आर्थिक असमानता भी एक बड़ा कारण है। आज भी बहुत से गाँवों में स्कूल भवन जर्जर हैं, शौचालय, बिजली, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं जैसी बुनियादी सुविधाएँ नहीं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर (अवसंरचना) की कमी भी एक बड़ा कारण है। यह भी एक कड़वा सच है कि आज शिक्षा से जुड़ी सरकारी योजनाएँ कागज़ों में तो अच्छी दिखती हैं, लेकिन उनका सही लाभ ज़मीनी स्तर तक नहीं पहुँचता। ग्रामीण इलाकों में आज भी शिक्षकों की कमी है, क्यों कि शिक्षक सुविधा अभाव के कारण आज भी गांवों में जाना नहीं चाहते हैं। दूसरी ओर, जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति रुचि का अभाव है तो इसके पीछे कारण गरीबी और आजीविका की चिंता है। ग्रामीणों को शिक्षा का कोई व्यावहारिक लाभ (पढ़ाई से नौकरी या कमाई) भी नहीं दिखता है और शायद यही वजह है कि वे शिक्षा को ज्यादा प्राथमिकता नहीं देते। ग्रामीणों में सामाजिक सोच और परंपराएं भी कहीं न कहीं आड़े आतीं हैं और वे ये समझते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, या खेती-किसानी, घर का ही असली काम है। इतना ही नहीं, डिजिटल शिक्षा या ऑनलाइन माध्यमों तक ग्रामीण छात्रों की पहुँच सीमित है, जिससे वे पीछे रह जाते हैं। प्रेरक वातावरण की कमी भी एक अन्य प्रमुख कारण है। अतः यह बात कही जा सकती है कि जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के संसाधनों का समान वितरण, शिक्षकों की नियमित नियुक्ति, और शिक्षा को रोजगार से जोड़ने वाले कार्यक्रम नहीं होंगे, तब तक यह असमानता बनी रहेगी। शिक्षा के प्रति रुचि तभी बढ़ेगी जब ग्रामीण समाज को यह महसूस होगा कि शिक्षा जीवन सुधार का सबसे सशक्त साधन है। बहरहाल, यह बहुत ही बड़ी बात है कि हमारे देश में एक लाख से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं, जो सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे ही चल रहे है। कहना ग़लत नहीं होगा कि प्रारंभिक या प्राथमिक शिक्षा बच्चों के भविष्य की असली नींव होती है। यही वह दौर होता है जब बच्चे जीवन के मूल संस्कार, आदतें और ज्ञान की बुनियादी समझ प्राप्त करते हैं। इस स्तर पर दी गई शिक्षा उनके सोचने-समझने और सीखने की क्षमता को विकसित करती है। यदि नींव मजबूत होगी तो आगे की शिक्षा भी सशक्त होगी। सच तो यह है कि प्राथमिक शिक्षा बच्चे में अनुशासन, आत्मविश्वास और जिज्ञासा का विकास करती है। यह उन्हें समाज में सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। एक अच्छी प्रारंभिक शिक्षा बच्चे को योग्य नागरिक बनने की राह पर अग्रसर करती है। इसलिए हर बच्चे के लिए गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है, लेकिन जब यह नींव ही कमजोर होगी तो फिर बच्चों का भविष्य कैसा होगा, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है।
दरअसल,देश में शिक्षा संसाधनों के असमान वितरण और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति रुचि के अभाव के पीछे कई गहरे और आपस में जुड़े हुए कारण हैं। मसलन, जहां शिक्षा संसाधनों के असमान वितरण की बात है तो आज शहरों में बहुत से अच्छे स्कूल स्थित हैं, उनमें बच्चों के लिए आधुनिक सुविधाएं व अच्छा स्टाफ उपलब्ध है। वहीं दूसरी ओर गांवों के स्कूलों में संसाधन बहुत ही सीमित हैं। आर्थिक असमानता भी एक बड़ा कारण है। आज भी बहुत से गाँवों में स्कूल भवन जर्जर हैं, शौचालय, बिजली, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं जैसी बुनियादी सुविधाएँ नहीं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर (अवसंरचना) की कमी भी एक बड़ा कारण है। यह भी एक कड़वा सच है कि आज शिक्षा से जुड़ी सरकारी योजनाएँ कागज़ों में तो अच्छी दिखती हैं, लेकिन उनका सही लाभ ज़मीनी स्तर तक नहीं पहुँचता। ग्रामीण इलाकों में आज भी शिक्षकों की कमी है, क्यों कि शिक्षक सुविधा अभाव के कारण आज भी गांवों में जाना नहीं चाहते हैं। दूसरी ओर, जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति रुचि का अभाव है तो इसके पीछे कारण गरीबी और आजीविका की चिंता है। ग्रामीणों को शिक्षा का कोई व्यावहारिक लाभ (पढ़ाई से नौकरी या कमाई) भी नहीं दिखता है और शायद यही वजह है कि वे शिक्षा को ज्यादा प्राथमिकता नहीं देते। ग्रामीणों में सामाजिक सोच और परंपराएं भी कहीं न कहीं आड़े आतीं हैं और वे ये समझते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, या खेती-किसानी, घर का ही असली काम है। इतना ही नहीं, डिजिटल शिक्षा या ऑनलाइन माध्यमों तक ग्रामीण छात्रों की पहुँच सीमित है, जिससे वे पीछे रह जाते हैं। प्रेरक वातावरण की कमी भी एक अन्य प्रमुख कारण है। अतः यह बात कही जा सकती है कि जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के संसाधनों का समान वितरण, शिक्षकों की नियमित नियुक्ति, और शिक्षा को रोजगार से जोड़ने वाले कार्यक्रम नहीं होंगे, तब तक यह असमानता बनी रहेगी। शिक्षा के प्रति रुचि तभी बढ़ेगी जब ग्रामीण समाज को यह महसूस होगा कि शिक्षा जीवन सुधार का सबसे सशक्त साधन है। बहरहाल, यह बहुत ही बड़ी बात है कि हमारे देश में एक लाख से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं, जो सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे ही चल रहे है। कहना ग़लत नहीं होगा कि प्रारंभिक या प्राथमिक शिक्षा बच्चों के भविष्य की असली नींव होती है। यही वह दौर होता है जब बच्चे जीवन के मूल संस्कार, आदतें और ज्ञान की बुनियादी समझ प्राप्त करते हैं। इस स्तर पर दी गई शिक्षा उनके सोचने-समझने और सीखने की क्षमता को विकसित करती है। यदि नींव मजबूत होगी तो आगे की शिक्षा भी सशक्त होगी। सच तो यह है कि प्राथमिक शिक्षा बच्चे में अनुशासन, आत्मविश्वास और जिज्ञासा का विकास करती है। यह उन्हें समाज में सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। एक अच्छी प्रारंभिक शिक्षा बच्चे को योग्य नागरिक बनने की राह पर अग्रसर करती है। इसलिए हर बच्चे के लिए गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है, लेकिन जब यह नींव ही कमजोर होगी तो फिर बच्चों का भविष्य कैसा होगा, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है।
वास्तव में आज के समय में सबसे चिंताजनक स्थिति ग्रामीण इलाकों की है, जहां यदि शिक्षक हैं तो स्कूल नहीं है और यदि कहीं पर शिक्षक मौजूद हैं, तो वहां बच्चों के नामांकन का अभाव है। यह सब देश में शिक्षण व्यवस्था की कमजोरी की ही नहीं, बल्कि प्राथमिक शिक्षा के प्रति सरकारी उदासीनता का भी प्रतीक है। दूसरे शब्दों में कहें तो बिना नामांकन वाले स्कूल शिक्षा प्रणाली पर एक गहरा कुठाराघात हैं। ये स्कूल इस बात का प्रतीक हैं कि देश में शिक्षा योजनाएँ तो बनाई जाती हैं, लेकिन उनका धरातलीय क्रियान्वयन कमजोर है। जब किसी स्कूल में एक भी छात्र नामांकित नहीं होता, तो यह केवल शिक्षा विभाग की लापरवाही नहीं, बल्कि सामाजिक उदासीनता का भी परिणाम है। इससे न केवल विभिन्न सरकारी संसाधन ही व्यर्थ जाते हैं, बल्कि यह एक तरह से बच्चों के अधिकारों का हनन भी है। यह स्थिति बताती है कि शिक्षा केवल भवन और शिक्षकों की नियुक्ति तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि जन-जागरण, निगरानी और वास्तविक सहभागिता की भी आवश्यकता है। ऐसे स्कूल हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमारी शिक्षा नीति वास्तव में हर बच्चे तक पहुँच पा रही है या नहीं ? ऐसा भी नहीं है कि आज शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए सरकारी योजनाओं का अभाव है।न ही स्कूलों में शिक्षकों की कमी ही है।एक बड़ी समस्या यह है कि आज विभिन्न सरकारी स्कूलों में शिक्षक नियुक्त तो हैं, लेकिन आज भी शिक्षक समय पर स्कूल नहीं पहुंचते हैं, वास्तव में नियुक्ति के बाद भी शिक्षकों का स्कूल नहीं पहुंचना इस समस्या(कम नामांकन या शून्य नामांकन) की जड़ में है। आज दानदाता और भामाशाह भी स्कूलों को भवन, टायलेट, पानी की सुविधा, लाइब्रेरी, मैदान आदि तक उपलब्ध कराते हैं,
लेकिन विडंबना ही है कि इनमें बच्चों का दाखिला हो इसकी चिंता कोई नहीं करता। आज हमारे देश में अक्सर यह देखा जाता है कि हमारे यहां सरकारी स्कूलों में बच्चों का नामांकन कम और प्राइवेट स्कूलों में अधिक होने के पीछे कई प्रमुख कारण हैं। सबसे पहले, सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षकों की लगातार अनुपस्थिति और संसाधनों की कमी अक्सर अभिभावकों को निराश करती है। कई जगहों पर स्कूल भवन जर्जर हैं, यहां तक कि टीन शैड के नीचे स्कूल संचालित करने की खबरें अक्सर मीडिया की सुर्खियों में पढ़ने को मिलती रहतीं हैं, इन स्कूलों में साफ-सफाई और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव देखने को मिलता है। दूसरी ओर, प्राइवेट स्कूल आकर्षक वातावरण, अंग्रेज़ी माध्यम, नियमित शिक्षण, और अनुशासन पर विशेष ध्यान देते हैं, जिससे अभिभावक उन्हें सरकारी स्कूलों की तुलना में कहीं अधिक बेहतर विकल्प मानते हैं। इसके अलावा, समाज में अंग्रेज़ी शिक्षा को लेकर बढ़ती मानसिकता भी कहीं न कहीं निजी स्कूलों की लोकप्रियता को बढ़ाती है। सरकारी स्कूलों में जिम्मेदारी और निगरानी की कमी के कारण भरोसा घटा है, जबकि निजी स्कूलों में परिणामों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। यही कारण है कि आज अधिकतर अभिभावक अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए प्राइवेट स्कूलों की ओर झुक रहे हैं। बहरहाल, आज सरकार स्कूलों का विलय करती है। दरअसल, कमजोर स्थिति में स्कूलों का विलय एक समाधान के रूप में देखा जाता है, लेकिन विलय कोई स्थाई समाधान नहीं है। वास्तव में, सरकारी स्कूलों के विलय से कई गंभीर नुकसान सामने आए हैं।पहला तो यह कि, दूर-दराज़ के ग्रामीण इलाकों में बच्चों को अब अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।विशेष रूप से बालिकाओं के लिए यह स्थिति और भी कठिन हो जाती है, क्योंकि सुरक्षा और सुविधाओं की कमी के कारण वे आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पातीं। यह भी कि एकीकृत स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ने से शिक्षकों पर बोझ बढ़ता है और प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन हो जाता है और इससे शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आती है। वहीं, जिन गाँवों के स्कूल बंद हो जाते हैं, वहाँ की स्थानीय पहचान और समुदाय का जुड़ाव भी समाप्त हो जाता है। अभिभावक भी बच्चों की शिक्षा पर निगरानी नहीं रख पाते, क्योंकि स्कूल अब दूर हो गया है। इसके अलावा, बंद पड़े स्कूल भवन धीरे-धीरे जर्जर होकर बेकार हो जाते हैं। गरीब परिवारों पर परिवहन और भोजन का अतिरिक्त बोझ बढ़ता है, जिससे शिक्षा महंगी और असुविधाजनक हो जाती है। कुल मिलाकर, स्कूलों का विलय शिक्षा की पहुंच, गुणवत्ता और सामाजिक जुड़ाव-तीनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। बहरहाल, कहना ग़लत नहीं होगा कि सरकारी स्कूलों के इस स्थिति (कम नामांकन) में पहुंचने के और भी कई कारण है। मसलन, आज अधिकांश अभिभावक, माता-पिता यह सोचते हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की शिक्षा और अनुशासन पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। सच तो यह है कि इसके लिए लोगों की सरकारी स्कूलों के प्रति ग़लत मानसिकता भी कहीं न कहीं जिम्मेदार है। आज अभिभावकों में यह धारणा घर कर गई है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बहुत गिर चुका है। इसलिए जिनके पास थोड़े भी संसाधन हैं, वे अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजना पसंद करते हैं। नतीजतन, आज सरकारी स्कूल खाली होते जा रहे हैं और उनकी प्रासंगिकता पर सवाल उठने लगे हैं।
वास्तव में, अभिभावकों और बच्चों को सरकारी स्कूलों से जोड़ने के लिए आज सबसे पहले इन स्कूलों की छवि और गुणवत्ता में सुधार बहुत ही जरूरी व आवश्यक हो गया है। सरकार को यह चाहिए कि वह स्कूलों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करे। स्कूलों में साफ-सफाई, खेलकूद, तकनीकी शिक्षा और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चे रुचि से सीख सकें या यूं कहें कि उनको अधिगम(लर्निंग) हो सके।अभिभावकों के साथ निरंतर संवाद स्थापित कर उन्हें यह बताया जाना चाहिए कि सरकारी स्कूल अब पहले जैसे नहीं रहे हैं, बल्कि बच्चों के समग्र विकास(आल राउंड डेवलपमेंट) के लिए बेहतर अवसर प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही, समाज में यह संदेश फैलाना होगा कि सरकारी शिक्षा केवल गरीबों के लिए नहीं, बल्कि सभी वर्गों के बच्चों के लिए समान रूप से उपयोगी है। जब सरकारी स्कूलों में विश्वास, गुणवत्ता और सुविधा बढ़ेगी, तो अभिभावक स्वाभाविक रूप से अपने बच्चों का दाखिला वहीं कराना पसंद करेंगे। सरकार को सरकारी स्कूलों को बेहतरीन बनाने के लिए इच्छाशक्ति का परिचय देना होगा और धरातल पर काम करना होगा। व्यवस्थाओं को पारदर्शी और अच्छा बनाने की दिशा में काम करना होगा। शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा।साथ ही हर जिले में मॉडल सरकारी स्कूल स्थापित करने होंगे। दरअसल, इन स्कूलों में आधुनिक तकनीक, स्मार्ट क्लासरूम, लैब, पुस्तकालय और प्रशिक्षित शिक्षकों की सुविधा उपलब्ध होती है। यहां छात्रों को केवल पाठ्यक्रम की पढ़ाई ही नहीं, बल्कि जीवन कौशल, खेल-कूद, कला और नवाचार के अवसर भी मिलते हैं। इसलिए इन स्कूलों की स्थापना से आम लोग अपने बच्चों को इन स्कूलों में एडमिशन दिलाने के लिए प्रोत्साहित होंगे और नामांकन बढ़ेगा। अंत में यही कहूंगा कि अगर प्रशासन, पंचायतें, अभिभावक और गांव के लोग मिलकर ठान लें कि बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाना है, तो स्कूलों की हालत जल्दी सुधर सकती है। वास्तव में यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी मिलकर स्कूल की व्यवस्था पर ध्यान रखें। वास्तव में इससे शिक्षकों और छात्रों दोनों में जिम्मेदारी की भावना बढ़ेगी। कहना ग़लत नहीं होगा कि नियमित निगरानी से शिक्षा की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। सरकारी स्कूल फिर से भरोसेमंद बन सकते हैं। जब समाज साथ देगा, तो बदलाव खुद दिखेगा। बच्चों का भविष्य मजबूत होगा और देश आगे बढ़ेगा।