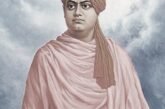आज एआइ (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का जमाना है। दुनिया में आज एआइ के प्रति प्यास निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, क्यों कि आज शिक्षा, स्वास्थ्य (हेल्थकेयर), खेती-किसानी, सुरक्षा, बैंकिंग और वित्त, उधोग और निर्माण (इंडस्ट्री एंड मैनुफैक्चरिंग), परिवहन,घर और दैनिक जीवन , मनोरंजन के क्षेत्रों में, सरकारी सेवाओं (गर्वनेंस), पर्यावरण संरक्षण से लेकर हर क्षेत्र में एआइ का बोलबाला हो गया है। मनुष्य धीरे धीरे ही सही एआइ के शिकंजे में फंसता चला जा रहा है। सच तो यह है कि आज दिमाग से तकनीक की दोस्ती लगातार बढ़ रही है। कहा गया है कि विज्ञान वरदान है तो अभिशाप भी है, इसलिए एआइ का उपयोग भी , मानव को विवेकपूर्ण तरीके/ढंग से करना चाहिए, क्यों कि इसके अनेक लाभ भी हैं तो हानियां भी हैं। सबसे बड़ी बात, हमें इस बात का ज़रा सा भी भान नहीं है कि एआइ हमारे नीले ग्रह का पानी सोख रही है। आज मनुष्य एआइ का आदी होता चला जा रहा है और वह कोई भी प्रश्न तकनीक से यानी कि एआइ की सहायता से पूछने लगा है, लेकिन एआइ से पूछा गया एक-एक सवाल लीटरों पानी की खपत कर रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो एआइ के कारण आज पानी का फुटप्रिंट या यूं कहें कि पानी का इस्तेमाल विस्फोटक ढंग से बढ़ता चला जा रहा है। पाठकों को जानकारी प्राप्त करके हैरानी होगी कि दुनिया भर के डेटा सेंटर हर साल अरबों लीटर पानी कूलिंग सिस्टम में सोख लेते हैं, और 2022–23 के बीच एआई ढांचे की जल-खपत में 30–40% की तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई। भारत में भी नए डेटा सेंटरों के कारण जल-उपयोग मेगालिटर स्तर तक बढ़ने लगा है। यदि एआई का ऐसे ही अंधाधुंध विस्तार होता रहा, तो यह भूजल स्तर को खतरनाक रूप से गिरा सकता है। इसलिए ‘सस्टेनेबल एआई’ की तकनीकों, ऊर्जा-कुशल मॉडल तथा जिम्मेदार उपयोग की ओर तत्काल कदम बढ़ाना ही धरती को जल-संकट से बचाने का एकमात्र रास्ता है। बहरहाल, यहां पाठकों को बताता चलूं कि एआई और पानी का फुटप्रिंट का आपस में संबंध है। दरअसल, आज के समय में एआई के बढ़ते उपयोग के साथ पानी की खपत पर कम चर्चा किया गया, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा बनकर उभर रहा है।
 गौरतलब है कि आधुनिक एआई मॉडल-खासकर बड़े लैंग्वेज मॉडल (एलएलएमएज) को ट्रेन करने और चलाने में भारी ऊर्जा के साथ-साथ काफी पानी भी लगता है। अब यहां प्रश्न यह उठता है कि आखिर एआई को पानी क्यों चाहिए ? तो इसका सीधा सा उत्तर यह है कि एआई मॉडल्स की ट्रेनिंग और इंफरेंस (रनिंग) शक्तिशाली डेटा सेंटरों में होता है। यह डेटा सेंटर 24×7 कंप्यूटिंग के कारण बहुत गर्म हो जाते हैं, इसलिए इन्हें ठंडा करने के लिए बड़ी मात्रा में पानी का उपयोग किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार पानी दो तरह से लगता है। मसलन, एक तो कूलिंग के लिए सीधे पानी का उपयोग किया जाता है। दरअसल, कूलिंग टावर्स में पानी वाष्पीकृत किया जाता है ताकि सर्वर ठंडे रह सकें। दूसरा यह कि विद्युत उत्पादन में भी अप्रत्यक्ष रूप से पानी का उपयोग होता है।दरअसल, बिजली उत्पादन-कोयला/थर्मल/न्यूक्लियर भी काफी पानी खर्च करता है। न केवल पानी बल्कि एआई-डेटा सेंटरों की वजह से ऊर्जा की खपत भी बहुत तेजी से बढ़ रही है।उदाहरण के लिए, एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में डेटा सेंटरों की बिजली खपत लगभग 487 टीडब्ल्यूएच (टेरावॉट-घंटा) थी और एई-विशिष्ट (एआइ) वर्कलोड के कारण यह खपत 50 टेरावॉट घंटा के आसपास थी और 2030 तक यह 554 टेरावॉट घंटा तक पहुंचने का अनुमान है। यहां पाठकों को बताता चलूं कि कि टेरावॉट घंटा ऊर्जा की एक बड़ी इकाई है, जिसका उपयोग बहुत बड़े पैमाने पर बिजली खपत या उत्पादन बताने के लिए किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो एक टेरावॉट घंटा से तात्पर्य एक अरब किलोवाट-घंटे से होता है। बहरहाल,पानी की खपत की बात करें तो, 2023 में डेटा सेंटरों ने लगभग 175 बिलियन लीटर पानी का उपयोग किया, और 2030 तक यह अनुमान 664 बिलियन लीटर तक पहुंचने का है।
गौरतलब है कि आधुनिक एआई मॉडल-खासकर बड़े लैंग्वेज मॉडल (एलएलएमएज) को ट्रेन करने और चलाने में भारी ऊर्जा के साथ-साथ काफी पानी भी लगता है। अब यहां प्रश्न यह उठता है कि आखिर एआई को पानी क्यों चाहिए ? तो इसका सीधा सा उत्तर यह है कि एआई मॉडल्स की ट्रेनिंग और इंफरेंस (रनिंग) शक्तिशाली डेटा सेंटरों में होता है। यह डेटा सेंटर 24×7 कंप्यूटिंग के कारण बहुत गर्म हो जाते हैं, इसलिए इन्हें ठंडा करने के लिए बड़ी मात्रा में पानी का उपयोग किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार पानी दो तरह से लगता है। मसलन, एक तो कूलिंग के लिए सीधे पानी का उपयोग किया जाता है। दरअसल, कूलिंग टावर्स में पानी वाष्पीकृत किया जाता है ताकि सर्वर ठंडे रह सकें। दूसरा यह कि विद्युत उत्पादन में भी अप्रत्यक्ष रूप से पानी का उपयोग होता है।दरअसल, बिजली उत्पादन-कोयला/थर्मल/न्यूक्लियर भी काफी पानी खर्च करता है। न केवल पानी बल्कि एआई-डेटा सेंटरों की वजह से ऊर्जा की खपत भी बहुत तेजी से बढ़ रही है।उदाहरण के लिए, एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में डेटा सेंटरों की बिजली खपत लगभग 487 टीडब्ल्यूएच (टेरावॉट-घंटा) थी और एई-विशिष्ट (एआइ) वर्कलोड के कारण यह खपत 50 टेरावॉट घंटा के आसपास थी और 2030 तक यह 554 टेरावॉट घंटा तक पहुंचने का अनुमान है। यहां पाठकों को बताता चलूं कि कि टेरावॉट घंटा ऊर्जा की एक बड़ी इकाई है, जिसका उपयोग बहुत बड़े पैमाने पर बिजली खपत या उत्पादन बताने के लिए किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो एक टेरावॉट घंटा से तात्पर्य एक अरब किलोवाट-घंटे से होता है। बहरहाल,पानी की खपत की बात करें तो, 2023 में डेटा सेंटरों ने लगभग 175 बिलियन लीटर पानी का उपयोग किया, और 2030 तक यह अनुमान 664 बिलियन लीटर तक पहुंचने का है।
मोर्गन स्टेनले की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2028 तक एआइ-डेटा सेंटरों की पानी की खपत (कूलिंग + बिजली उत्पादन) 1,068 बिलियन लीटर पहुँच सकती है, जो 2024 के स्तर से लगभग 11 गुना अधिक है। वहीं दूसरी ओर यदि हम ऊर्जा की खपत की ओर देखें तो, आज के एआइ वर्कलोडों में काफी तेजी से वृद्धि हो रही है। दरअसल, बड़े मॉडल-ट्रेनिंग से लेकर रोज़मर्रा की इनफेरेंस (प्राप्ति) वर्कलोड तक, दोनों ही ऊर्जा माँग को बढ़ा रहे हैं। आज भारत जैसे विकासशील देश में एआई-डेटा सेंटर्स की तेजी से वृद्धि हो रही है, जिसके कारण ऊर्जा और पानी पर दबाव बढ़ रहा है।एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में एआई-डेटा सेंटर्स की बिजली की मांग 2030 तक लगभग 50 टीडब्ल्यूएच प्रति वर्ष तक पहुंच सकती है।पानी की खपत को लेकर एक्वार्टिया नाम की ब्लॉग रिपोर्ट कहती है कि भारत का डेटा सेंटर पानी उपयोग 2025 में लगभग 150.30 बिलियन लीटर था, जो 2029 तक बढ़कर 358.66 बिलियन लीटर तक पहुँच सकता है। इसके अलावा, बिज़नेस स्टैंडर्ड में एक लेख में बताया गया है कि भारत में डेटा सेंटर क्षमता बहुत तेज़ी से बढ़ रही है (2027 तक 1.8 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान), और इससे ऊर्जा-पानी दोनों संसाधनों पर दबाव बढ़ सकता है। यहां पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि 1 गीगावाट 1,000 मेगावाट और 1 मेगावाट 1,000 किलोवाट के बराबर होता है। इसलिए 1.8 जीडब्लयू का मतलब 1,800 मेगावाट या 18,00,000 किलोवाट हुआ, जो बहुत बड़ी मात्रा की बिजली है, जितनी ऊर्जा बड़े बिजली संयंत्र या पूरे शहर की बड़ी आबादी चला सकती है। बहरहाल,एक अन्य उपलब्ध जानकारी के अनुसार एआई-वर्कलोड की वजह से डेटा सेंटर्स की ऊर्जा खपत पिछले कुछ सालों में लगभग 20% प्रतिवर्ष बढ़ी है। तक्षशिला इंस्टीट्यूशन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में डेटा सेंटर्स में ठंडा करने (कूलिंग) के लिए पानी की खपत, भारतीय जलवायु की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लगभग 25.5 मिलियन लीटर प्रति मेगावॉट (एमडब्लयू) प्रति वर्ष हो सकती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कई डेटा सेंटर ऑपरेटर ऊर्जा और पानी की खपत के संदर्भ में अपने आंकड़े भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं दे रहे हैं। बहरहाल, आज हमारे देश में डेटा सेंटर की कुल क्षमता बहुत तेजी से बढ़ रही है। टीबीएस(द बिजनेस स्टैंडर्ड ) की एक रिपोर्ट कहती है कि 2027 तक भारत की डेटा सेंटर क्षमता 1.8 जीडब्लयू तक पहुँच सकती है, जिससे बिजली की मांग बहुत बढ़ेगी। आज बहुत सी डेटा कंपनियां हैं,जो अपने सटीक ‘डेटा-सेंटर-स्तर’ ऊर्जा खपत और जल उपयोग को इएसजी (एनवायरमेंटल, सोशल एंड गर्वनेंस) रिपोर्ट में खुलकर नहीं दिखातीं। दरअसल, इस मुद्दे पर पारदर्शिता में कमी है। हाल फिलहाल, कहना ग़लत नहीं होगा कि भारत में एआई के बढ़ते इस्तेमाल से बिजली और पानी की खपत तेज़ी से बढ़ रही है। एआई चलाने वाले डेटा सेंटर और क्लाउड सर्वर बहुत अधिक बिजली खपत करते हैं, क्योंकि दिन-रात हजारों कंप्यूटर चलते रहते हैं। बड़े एआई मॉडल को ट्रेन करने में हजारों घरों जितनी बिजली लग सकती है। दरअसल, सर्वरों को ठंडा रखने के लिए बहुत पानी चाहिए, इसलिए पानी की खपत भी बढ़ रही है । एक कंप्यूट यूनिट को चलाने में सैकड़ों लीटर पानी खर्च हो सकता है। चूंकि, भारत में डिजिटल सेवाएँ, एआई कंपनियाँ और क्लाउड सिस्टम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसलिए ऊर्जा और पानी की यह माँग आगे और भी बढ़ेगी। इसी वजह से अब सौर ऊर्जा, हरित बिजली और पानी-कुशल डेटा सेंटर की जरूरत पहले से कहीं ज़्यादा हो गई है।
 अंत में यही कहूंगा कि एआई मॉडलों का पानी-फुटप्रिंट तेजी से बढ़ती डिजिटल दुनिया की एक गंभीर पर्यावरणीय चुनौती बनता जा रहा है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि बड़े एआई मॉडल-जैसे जीपीटी-4 आकार के मॉडल को ट्रेन करने में कई लाख लीटर पानी खर्च हो सकता है, जबकि चैटजीपीटी जैसे मॉडलों से 20-50 सवाल पूछने भर में उतना पानी लग जाता है, जितना एक कप चाय बनाने में लगता है। जानकारी के अनुसार यह खपत डेटा सेंटर की लोकेशन, मौसम और कूलिंग तकनीक पर निर्भर करती है। एआई उपयोग बढ़ने का सीधा असर पानी की मांग पर पड़ता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पहले से जल-संकट है। डेटा सेंटर, ऊर्जा उपयोग और पानी की खपत मिलकर एक त्रिकोणीय दबाव बनाते हैं, जिससे टेक कंपनियों के लिए पर्यावरणीय निगरानी और भी जरूरी हो जाती है। इस चुनौती को देखते हुए गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियाँ ‘वाटर पाज़ीटिव’ बनने का लक्ष्य लेकर चल रही हैं और एयर-कूलिंग, इमर्शन कूलिंग व रीसाइकल्ड पानी जैसे समाधान अपना रही हैं। जैसा कि ऊपर भी बता चुका हूं कि भारत में भी एआई और डेटा सेंटरों का विस्तार तेजी से हो रहा है, लेकिन कई राज्यों में पहले से पानी की कमी होने के कारण स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इसलिए भविष्य में ऊर्जा-कुशल एआई मॉडल, नवीकरणीय ऊर्जा आधारित डेटा सेंटर, पारदर्शी पानी उपयोग रिपोर्टिंग और स्थानीय जल संरक्षण में टेक कंपनियों की सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी होगी। समग्र रूप से देखा जाए तो एआई का बढ़ता जल-फुटप्रिंट एक अहम पर्यावरणीय चेतावनी है, और तकनीक को जिम्मेदार व टिकाऊ बनाकर ही संतुलित विकास संभव है।निष्कर्षतः, एआई का बढ़ता जल-फुटप्रिंट हमें यह याद दिलाता है कि तकनीकी प्रगति के साथ पर्यावरणीय जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बड़े एआई मॉडलों में भारी पानी और ऊर्जा खपत भविष्य के लिए चिंता का विषय है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पहले से ही जल-संकट मौजूद है। इसलिए बहुत ही जरूरी और आवश्यक है कि डेटा सेंटर अधिक कुशल कूलिंग तकनीक अपनाएँ। टेक कंपनियाँ पानी-कार्बन न्यूट्रल लक्ष्यों पर गंभीरता से काम करें, और सरकारें टिकाऊ एआई नीतियाँ विकसित करें। आज एआई के बढ़ते उपयोग से डेटा सेंटरों में ऊर्जा और पानी की खपत तेजी से बढ़ रही है, जिससे हमारे नीले ग्रह के जल संसाधनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम चाहें तो इस समस्या को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।पहला तो यह कि हमें एआई सेवाओं का समझदारी से उपयोग करना चाहिए तथा इसके अति-उपयोग से बचना चाहिए।दूसरा, कंपनियों और सरकारों पर ग्रीन डेटा सेंटर, पुनर्चक्रित पानी और नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने का दबाव बनाकर समस्या को काफी हद तक हल किया जा सकता है। तीसरा, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को कम-ऊर्जा और कम-पानी वाले एआई मॉडल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।चौथा, डिजिटल स्वच्छता-अनावश्यक स्टोरेज, बेकार डेटा और पुराने फ़ाइलों को हटाना-सीधे संसाधन खपत कम करता है। पाँचवा, उपयोगकर्ता के रूप में हम उन प्लेटफॉर्मों का समर्थन करें जो सस्टेनेबल एआई के सिद्धांत अपनाते हैं। छठा, घर-समाज में पानी संरक्षण को बढ़ावा देकर ग्रह पर कुल जल-दबाव घटाया जा सकता है। सातवां, तकनीक और पर्यावरण शिक्षा से जागरूक नागरिक तैयार हों। आख़िरकार, एआई मानवता की सुविधा के लिए है, लेकिन तभी तक जब तक हम इसे ज़िम्मेदारी और संतुलन के साथ इस्तेमाल करना सीखते हैं। वास्तव में, हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि केवल जिम्मेदार तकनीकी उपयोग और संसाधनों के संरक्षण के माध्यम से ही हम एआई के लाभों का आनंद लेते हुए एक संतुलित और स्थायी भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।
अंत में यही कहूंगा कि एआई मॉडलों का पानी-फुटप्रिंट तेजी से बढ़ती डिजिटल दुनिया की एक गंभीर पर्यावरणीय चुनौती बनता जा रहा है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि बड़े एआई मॉडल-जैसे जीपीटी-4 आकार के मॉडल को ट्रेन करने में कई लाख लीटर पानी खर्च हो सकता है, जबकि चैटजीपीटी जैसे मॉडलों से 20-50 सवाल पूछने भर में उतना पानी लग जाता है, जितना एक कप चाय बनाने में लगता है। जानकारी के अनुसार यह खपत डेटा सेंटर की लोकेशन, मौसम और कूलिंग तकनीक पर निर्भर करती है। एआई उपयोग बढ़ने का सीधा असर पानी की मांग पर पड़ता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पहले से जल-संकट है। डेटा सेंटर, ऊर्जा उपयोग और पानी की खपत मिलकर एक त्रिकोणीय दबाव बनाते हैं, जिससे टेक कंपनियों के लिए पर्यावरणीय निगरानी और भी जरूरी हो जाती है। इस चुनौती को देखते हुए गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियाँ ‘वाटर पाज़ीटिव’ बनने का लक्ष्य लेकर चल रही हैं और एयर-कूलिंग, इमर्शन कूलिंग व रीसाइकल्ड पानी जैसे समाधान अपना रही हैं। जैसा कि ऊपर भी बता चुका हूं कि भारत में भी एआई और डेटा सेंटरों का विस्तार तेजी से हो रहा है, लेकिन कई राज्यों में पहले से पानी की कमी होने के कारण स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इसलिए भविष्य में ऊर्जा-कुशल एआई मॉडल, नवीकरणीय ऊर्जा आधारित डेटा सेंटर, पारदर्शी पानी उपयोग रिपोर्टिंग और स्थानीय जल संरक्षण में टेक कंपनियों की सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी होगी। समग्र रूप से देखा जाए तो एआई का बढ़ता जल-फुटप्रिंट एक अहम पर्यावरणीय चेतावनी है, और तकनीक को जिम्मेदार व टिकाऊ बनाकर ही संतुलित विकास संभव है।निष्कर्षतः, एआई का बढ़ता जल-फुटप्रिंट हमें यह याद दिलाता है कि तकनीकी प्रगति के साथ पर्यावरणीय जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बड़े एआई मॉडलों में भारी पानी और ऊर्जा खपत भविष्य के लिए चिंता का विषय है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पहले से ही जल-संकट मौजूद है। इसलिए बहुत ही जरूरी और आवश्यक है कि डेटा सेंटर अधिक कुशल कूलिंग तकनीक अपनाएँ। टेक कंपनियाँ पानी-कार्बन न्यूट्रल लक्ष्यों पर गंभीरता से काम करें, और सरकारें टिकाऊ एआई नीतियाँ विकसित करें। आज एआई के बढ़ते उपयोग से डेटा सेंटरों में ऊर्जा और पानी की खपत तेजी से बढ़ रही है, जिससे हमारे नीले ग्रह के जल संसाधनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम चाहें तो इस समस्या को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।पहला तो यह कि हमें एआई सेवाओं का समझदारी से उपयोग करना चाहिए तथा इसके अति-उपयोग से बचना चाहिए।दूसरा, कंपनियों और सरकारों पर ग्रीन डेटा सेंटर, पुनर्चक्रित पानी और नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने का दबाव बनाकर समस्या को काफी हद तक हल किया जा सकता है। तीसरा, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को कम-ऊर्जा और कम-पानी वाले एआई मॉडल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।चौथा, डिजिटल स्वच्छता-अनावश्यक स्टोरेज, बेकार डेटा और पुराने फ़ाइलों को हटाना-सीधे संसाधन खपत कम करता है। पाँचवा, उपयोगकर्ता के रूप में हम उन प्लेटफॉर्मों का समर्थन करें जो सस्टेनेबल एआई के सिद्धांत अपनाते हैं। छठा, घर-समाज में पानी संरक्षण को बढ़ावा देकर ग्रह पर कुल जल-दबाव घटाया जा सकता है। सातवां, तकनीक और पर्यावरण शिक्षा से जागरूक नागरिक तैयार हों। आख़िरकार, एआई मानवता की सुविधा के लिए है, लेकिन तभी तक जब तक हम इसे ज़िम्मेदारी और संतुलन के साथ इस्तेमाल करना सीखते हैं। वास्तव में, हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि केवल जिम्मेदार तकनीकी उपयोग और संसाधनों के संरक्षण के माध्यम से ही हम एआई के लाभों का आनंद लेते हुए एक संतुलित और स्थायी भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।